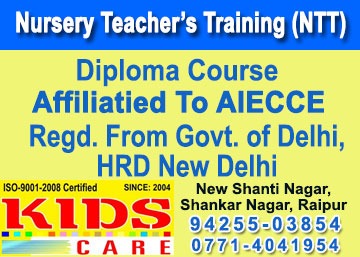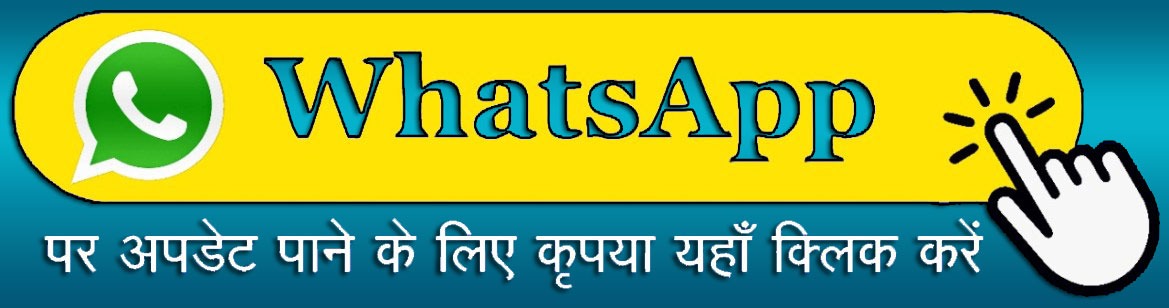भारतीय इतिहास में 14 अक्टूबर 1956 का दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है, जब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपने 365,000 दलित अनुयायियों के साथ हिंदू धर्म त्यागकर बौद्ध धर्म को अपनाया। पूरा घटनाक्रम समझिए।
“दुर्भाग्यवश मैं हिंदू अछूत के रूप में जन्मा, यह मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं नीच और अपमानजनक स्थिति में जीना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं आपको यह दृढ़ आश्वासन देता हूं कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं।”- ये शब्द डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में आयोजित सम्मेलन में कहे थे। इस घोषणा ने न केवल हिंदू समाज के भीतर हलचल मचा दी, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ स्थापित किया।
हालांकि उन्होंने यह ऐलान 1935 में किया, लेकिन अंतिम निर्णय तक पहुंचने में उन्हें दो दशक से अधिक समय लगा। इस अवधि में उन्होंने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया, दलित अधिकारों की वकालत की और विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया। अंततः उन्हें समता और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित बौद्ध धर्म में मुक्ति का मार्ग दिखाई दिया।
ऐतिहासिक निर्णय की नींव 1936 में रखी गई
आज 14 अक्टूबर है और यह दिन भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। ठीक 69 साल पहले, 1956 में इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़कर अपने 365,000 दलित अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। यह घटना न केवल उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ थी, बल्कि लाखों दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनी। अंबेडकर का यह कदम हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध का प्रतीक बना, जिसने सदियों से दलितों को सामाजिक और धार्मिक रूप से हाशिए पर रखा था। यह न केवल भारत, बल्कि विश्व इतिहास के सबसे बड़े धर्मांतरणों में से एक था।
इस ऐतिहासिक निर्णय की नींव 1936 में रखी गई जब अंबेडकर ने मुंबई के दादर में एक सम्मेलन आयोजित किया ताकि येवला घोषणा के बाद धर्म परिवर्तन आंदोलन पर जनसमर्थन का आकलन किया जा सके। इस सम्मेलन में करीब 35,000 महार समुदाय के लोग शामिल हुए।
अपने भाषण में अंबेडकर ने धर्म के दो पहलुओं- सामाजिक-धार्मिक और भौतिक-आध्यात्मिक पर विचार पेश किए। उन्होंने पूछा: धर्म का उद्देश्य क्या है? और यह क्यों आवश्यक है? अंबेडकर का मानना था कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिकता, समानता और स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाना है- न कि उसे किसी सामाजिक ढांचे में बांध देना।
डॉ. अंबेडकर का जन्म और शुरुआती जीवन: संघर्ष की नींव
अंबेडकर के बौद्ध धर्म अपनाने के फैसले को समझने से पहले उनके शुरुआती जीवन को समझना जरूरी है। डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक महार जाति के परिवार से थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। बचपन से ही उन्हें जाति-भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठना पड़ता था, पानी पीने के लिए अलग घड़ा रखा जाता था और यहां तक कि अध्यापक उन्हें छूने से डरते थे। लेकिन अंबेडकर बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी।
उनके पिता ब्रिटिश सेना में थे जिससे घर में शिक्षा का माहौल था। अंबेडकर ने बॉम्बे (अब मुंबई) से मैट्रिक पास की फिर बड़ौदा के महाराजा की मदद से अमेरिका और इंग्लैंड में उच्च शिक्षा हासिल की। वे अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति शास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। वापस भारत लौटकर उन्होंने वकील के रूप में काम शुरू किया, लेकिन जाति के कारण उन्हें मुश्किलें आईं। इस अनुभव ने उन्हें दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
जाति-व्यवस्था के खिलाफ जंग: एक योद्धा का उदय
भारत में उस समय हिंदू समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। दलितों को शूद्रों से भी नीचे माना जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, गांव के कुओं से पानी नहीं पी सकते थे और शिक्षा-रोजगार में भेदभाव होता था। अंबेडकर ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1920 के दशक में महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा। यह एक बड़ा आंदोलन था।
1930 में वे ब्रिटिश सरकार के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जहां उन्होंने दलितों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। महात्मा गांधी से उनका मतभेद था। गांधी दलितों को ‘हरिजन’ कहते थे और हिंदू समाज में सुधार चाहते थे, लेकिन अंबेडकर मानते थे कि हिंदू धर्म में जाति-व्यवस्था जड़ से जुड़ी है, इसलिए दलितों को अलग रास्ता अपनाना चाहिए। 1932 में पूना पैक्ट हुआ जिसमें दलितों को आरक्षण मिला, लेकिन अंबेडकर इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे।
1935 में, येवला सम्मेलन में अंबेडकर ने ऐलान किया: “मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं।” यह बयान पूरे देश में गूंजा। वे समझ चुके थे कि हिंदू धर्म में दलितों को समानता नहीं मिल सकती। उन्होंने दूसरे धर्मों का अध्ययन शुरू किया। ईसाई, इस्लाम, सिख और बौद्ध धर्म पर विचार किया। आखिरकार, उन्होंने बौद्ध धर्म चुना क्योंकि यह समानता, अहिंसा और बुद्धि पर जोर देता है, और जाति-व्यवस्था को नकारता है।
अंबेडकर का हिंदू धर्म के प्रति असंतोष
डॉ. अंबेडकर का हिंदू धर्म के प्रति असंतोष कोई नई बात नहीं थी। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की मूल संरचना, विशेष रूप से जाति व्यवस्था, भारतीय समाज में स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन से भी बड़ा खतरा है। जहां महात्मा गांधी जाति व्यवस्था में सुधार की वकालत करते थे, वहीं अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि दलितों के लिए भारतीय समाज में सम्मानजनक स्थान केवल धर्म परिवर्तन के माध्यम से ही संभव है। मई 1936 में, मुंबई में महार समुदाय की एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने कहा था, “मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से कहता हूं, धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। मानवीय व्यवहार पाने के लिए, धर्म परिवर्तन करो।”
बौद्ध धर्म का चयन: एक लंबी विचार प्रक्रिया
अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था। उन्होंने 20 वर्षों तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और यह तय करने में समय लिया कि कौन सा धर्म उनके और उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाने का विचार खारिज कर दिया, क्योंकि इन धर्मों को वे भारतीयता से अलग मानते थे। प्रोफेसर गौरी विश्वनाथन के अनुसार, अंबेडकर भारतीयता के दायरे में रहते हुए भी एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जो समानता और तर्क पर आधारित हो। अंततः, उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना और अपनी समझ के अनुरूप ‘नवयान’ बौद्ध धर्म की स्थापना की जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के कुछ हिस्सों को तर्क और आधुनिकता के आधार पर संशोधित किया।
वह ऐतिहासिक दिन: 14 अक्टूबर 1956, दीक्षा भूमि, नागपुर
अब आते हैं उस दिन पर, जिसे हम ‘आज का दिन’ कह रहे हैं। 1956 का भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़ चुका था। अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। उन्होंने संविधान में समानता, न्याय और आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन समाज में बदलाव धीमा था। दलित अभी भी दबाए जा रहे थे। अंबेडकर बीमार थे, लेकिन उन्होंने अपना फैसला लिया। 14 अक्टूबर 1956 को, विजयादशमी के दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक विशाल समारोह हुआ। अंबेडकर ने श्रीलंका से आए भिक्षु महास्थविर चंद्रमणि से बौद्ध दीक्षा ली। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लीं, जिनमें हिंदू देवी-देवताओं को न मानना, ब्राह्मणों को गुरु न मानना और बौद्ध सिद्धांतों का पालन करना शामिल था। उनके साथ उनकी पत्नी सविता अंबेडकर और करीब 5 लाख अनुयायी भी बौद्ध बने। यह दुनिया का सबसे बड़ा सामूहिक धर्मांतरण था। यह घटना क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ‘नवयान’ कहा, यानी नया रास्ता। उन्होंने पुराने बौद्ध ग्रंथों को सरल बनाया और किताब ‘द बुद्धा एंड हिज धम्मा’ लिखी, जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। इस धर्मांतरण ने दलितों को नई पहचान दी। वे अब खुद को ‘बौद्ध’ कह सकते थे, जो जाति से ऊपर था।
अंबेडकर की मृत्यु और विद्वानों की व्याख्या
दुर्भाग्यवश, अंबेडकर बौद्ध धर्म अपनाने के केवल दो महीने बाद ही 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु के बाद, विद्वानों ने उनके धर्म परिवर्तन के कारणों पर गहन विचार-विमर्श किया। इन कारणों को मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोणों में बांटा गया है:
राजनीतिक विरोध: कुछ विद्वानों, जैसे समाजशास्त्री गेल ओमवेट, का मानना है कि अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना एक राजनीतिक विरोध था। 1932 के पूना समझौते में अंबेडकर को अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद उनकी निराशा इस कदम में झलकती है।
हिंदू धर्म के खिलाफ आजीवन संघर्ष: अंबेडकर के जीवन में जाति आधारित भेदभाव का अनुभव बचपन से ही शुरू हो गया था। विद्वानों का मानना है कि उनका धर्म परिवर्तन उनके व्यक्तिगत अनुभवों और सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम था। दक्षिण भारत के 12वीं सदी के दलित संत नंदनार और सम्राट अशोक जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों ने उनके विचारों को आकार दिया। अंबेडकर ने कहा था, “हिंदू समाज समानता का व्यवहार नहीं करता, लेकिन धर्म परिवर्तन से यह आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।”
बौद्ध धर्म- आधुनिकता का प्रतीक: धर्म अध्ययन विशेषज्ञ क्रिस्टोफर क्वीन के अनुसार, अंबेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना आधुनिकता की ओर एक कदम था। उन्होंने बौद्ध धर्म को तर्क, नैतिकता और न्याय पर आधारित सबसे आधुनिक धर्म माना। अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को पुनर्व्याख्या करते हुए इसे और अधिक तर्कसंगत बनाया, जैसे कि ‘चार आर्य सत्य’ जैसे कुछ हिस्सों को हिंदू प्रभाव मानकर खारिज किया। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि अंबेडकर के बौद्ध धर्म में फ्रांसीसी क्रांति के मूल्य- स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व झलकते हैं।
दलित आंदोलन और बौद्ध धर्म का पुनर्जनन
अंबेडकर के धर्म परिवर्तन ने दलित आंदोलन को नई गति दी और भारत में बौद्ध धर्म को पुनर्जनन प्रदान किया। 1951 की जनगणना में भारत में बौद्धों की संख्या 141,426 थी, जो 1961 में बढ़कर 3,206,142 हो गई। यह वृद्धि अंबेडकर के नेतृत्व में हुए सामूहिक धर्म परिवर्तन का परिणाम थी।